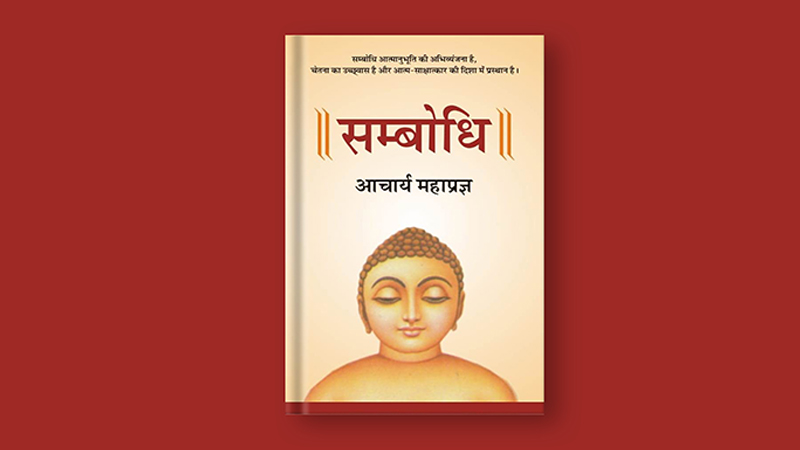
संबोधि
ु आचार्य महाप्रज्ञ ु
क्रिया-अक्रियावाद
(14) एवं शिक्षासमापन्नो, गृहवासेऽपि सुव्रत:।
अमेध्यं देहमुज्झित्वा, देवलोकं च गच्छति॥
इस प्रकार शिक्षा से संपन्न सुव्रती मनुष्य गृहवास में भी अशुचि शरीर को छोड़कर देवलोक में जाता है।
(15) दीर्घायुष ॠद्धिमन्त:, समृद्धा: कामरूपिण:।
अधुनोत्पन्नसंकाशा:, अर्चिमालिसमप्रभा:॥
(16) देवा दिवि भवन्त्येते, धर्मं स्पृशान्ति ये जना:।
अगारिणोऽनगारा वा, संयमस्तत्र कारणम्॥ (युग्मम्)
जो गृहस्थ या साधु धर्म की आराधना करते हैं, वे स्वर्ग में दीर्घायु, ॠद्धिमान्, समृद्ध, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, अभी उत्पन्न हुए होंऐसी कांति वाले और सूर्य के जैसी दीप्ति वाले देव होते हैं। उसका कारण संयम है।
संयम का मुख्य फल हैकर्म-निर्जरण, आत्म पवित्रता। उसका गौण फल हैदेवलोक आदि की प्राप्ति।
संयम आत्म-जागरण है। उसके आत्म-गुणों का उपबृंहण होता है। आत्मा के मूल गुण हैंअनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतचारित्र, सहज आनंद आदि-आदि संयम इन सबकी प्राप्ति का साधन है।
देवलोक आदि पौद्गलिक स्थितियों की प्राप्ति उसका सहचारी फल है। प्रस्तुत श्लोकों में उसी का प्रतिपादन है।
(17) सर्वथा संवृतो भिक्षु:, द्वयोरन्यतरो भवेत्।
कृत्स्नकर्मक्षयान्मुक्तो, देवो वापि महर्द्धिक:॥
जो भिक्षु सर्वथा संवृत हैकर्म-आगमन के हेतुओं का निरोध किए हुए है, वह इन दोनों में से किसी एक अवस्था को प्राप्त होता हैसब कर्मों का क्षय हो जाए तो वह मुक्त हो जाता है, अन्यथा समृद्धिशाली देव बनता है।
कारण के बिना कार्य की उपलब्धि नहीं होती। परिदृश्यमान जगत् कार्य है तो निस्संदेह उसका अदृश्य कारण भी होना चाहिए। तृष्णा, वासना या कर्म कारण है। कारण की परंपरा का निर्मूलन करना साधना का वास्तविक ध्येय है। कर्म से प्रवृत्ति-चंचलता पैदा होती है और चंचलता से पुन: कर्म का सृजन होता है। कर्म का यह क्रम टूटता नहीं हैं साधना उस क्रम को तोड़ने का शस्त्र है। साधक की साधना यदि प्रवृत्तिशून्यता की चरम सीमा का स्पर्श कर लेती है तो वह अयोगी (प्रवृत्ति-मुक्त) सर्व दु:खों से मुक्त हो जाता है। यदि प्रवृत्ति का क्रम पूर्णतया निरुद्ध नहीं हुआ है तो पुन: जन्म लेना उसके लिए अनिवार्य है। किंतु इस बीच वह अपने असीम पुण्य-बल से एक बार स्वर्ग में जन्म ले पुन: वहाँ से मनुष्य जीवन में अवतरित होता है। साधना का पुन: अवसर प्राप्त कर जीवन के सर्वोच्च विकास-शिखर को छू लेता है।
गीता में वर्णित योग-भ्रष्ट व्यक्ति के साथ इसका यत् किंचित् सामंजस्य किया जा सकता है।
योग-भ्रष्ट शब्द का अभिप्राय यह हो कि वह योग-मार्ग को पूर्णतया साध नहीं सका, तो यहाँ कोई भिन्नता जैसी बात नहीं रहती। यदि इसका अर्थयोग-मार्ग से च्युत हो या बीच में ही छोड़ दिया हो तो फिर दूसरी बात है। किंतु आगे के वर्णन से स्पष्ट है कि वह व्यक्ति किसी योनि में योग-कुल में आकर जन्म ग्रहण करता है और अपने अवशेष योग की साधना में संलग्न होकर उसे परिपूर्णतया साध लेता है।

