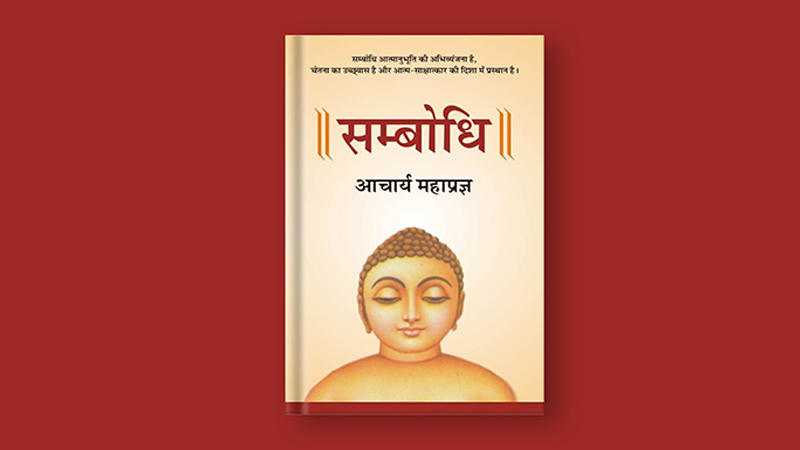
संबोधि
बंध-मोक्षवाद
भगवान् प्राह
(पिछला शेष) इससे मुक्त होकर ही साधक व्रतविरति की ओर अग्रसर होता है। विरति का अर्थ हैबाह्य विषयों से विरक्त होना। जिसका सीधा अर्थ हैवैराग्य यानी पदार्थों के प्रति जो अनुरक्ति है, उससे दूर होना। पदार्थों का आकर्षण, सुख-सुविधा का आकर्षण आत्मा के प्रति, परम तत्त्व के प्रति आकृष्ट नहीं होने देता। दोनों एक-दूसरे के विरोधी हैं। विरत अवस्था में पदार्थों-विषयों में आसक्ति छूट जाती है। आत्मा की दिशा में बढ़ने का मार्ग खुल जाता है। लेकिन वह मार्ग पूर्ण नहीं खुलता। मन कभी पदार्थों की ओर तथा कभी आत्मा की ओर चलता रहता है। इसके लिए साधक को बड़ा कठोर साहसिक कदम उठाना होता है। अपने मन पर उसे प्रहरी बनकर खड़ा रहना होता है, प्रतिपल जागृत होकर आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखना होता है। इस अस्थिरता का कारण होता हैप्रमाद। प्रमाद का आध्यात्मिक भाषा में अर्थ हैआत्मा के प्रति अनुत्साह, विषयों के प्रति उत्साह। प्रमाद की मुक्ति के लिए अप्रमाद का अवलंबन अपेक्षित है।
अनन्य के प्रति आकर्षण इतना सघन होना शुरू हो जाता है, तब उसे अन्य किसी बात का ख्याल नहीं रहता। वह सतत उसी में डूबा रहने लगता है। यह धारा जब विकास की अग्रिम अवस्था को छूने लगती है तब वह दो भागोंदो श्रेणियों में विभक्त हो जाती है। विकास की दृष्टि से अप्रमाद का स्थान सातवाँ है। सातवें से दो पथ बनते हैंएक उपशम श्रेणि का और दूसरा क्षायक श्रेणि का। उपशमन श्रेणि से जाने वाले ग्यारहवें में आकर रुक जाते हैं। जो साधक क्षयक श्रेणि के पथ से प्रयाण करते हैं वे सीधे दसवें से बारहवें में आरूढ़ हो जाते हैं। इसके बाद तेरहवें व चौदहवें गुणस्थान में प्रवेश कर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, सहजावस्था में अवस्थित हो जाते हैं। यह आत्मा के पूर्ण विकास की स्थिति है।
गुणस्थान चौदह हैं। गुणस्थान हैआत्मा के क्रमिक विकास का पथ। अविकास का कारण हैकर्म। गीता की दृष्टि में प्रकृति। प्रकृति की तीन अवस्थाएँ हैंसत्त्व, रज और तम। तीनों की अतीत अवस्था है। गुणातीत। करण श्रीर मूल है। इसी के कारण-स्थूल शरीर का निर्माण होता है। गुणातीत अवस्था में कारण शरीर की भी समाप्ति हो जाती है। जैसे-जैसे साधक साधना की उच्च अवस्था में या ध्यान की गहराई में आगे से आगे आरूढ़ होता रहता है वैसे-वैसे उसका मोह क्षय होता चला जाता है और वह पूर्ण विशुद्ध दशा में स्थित हो जाता है।
मोह आत्मा को विकृत करता है। उसके राग और द्वेषये दो रूप हैं। इन दोनों के चार रूप बनते हैंक्रोध, अहंकार, माया और लोभ। गुणस्थानों के आरोहण में क्रमश: ये शिथिल व नाम शेष होते चल जाते हैं। ग्यारहवें गुणस्थान में इनका संपूर्ण उपशमन होता है, नाश नहीं होता। बारहवें में संपूर्ण विलय-क्षय हो जता है।
(27) अमनोज्ञसमुत्पाद:, दु:खंभवति देहिनाम्।
समुत्पादमजनाना, न हि जानन्ति संवरम्॥
अनमोज्ञ स्थिति का समुत्पादउत्पत्ति दु:ख है। जो इस समुत्पाद को नहीं जानते, वे संवरदु:ख निरोध को भी नहीं जानते।

